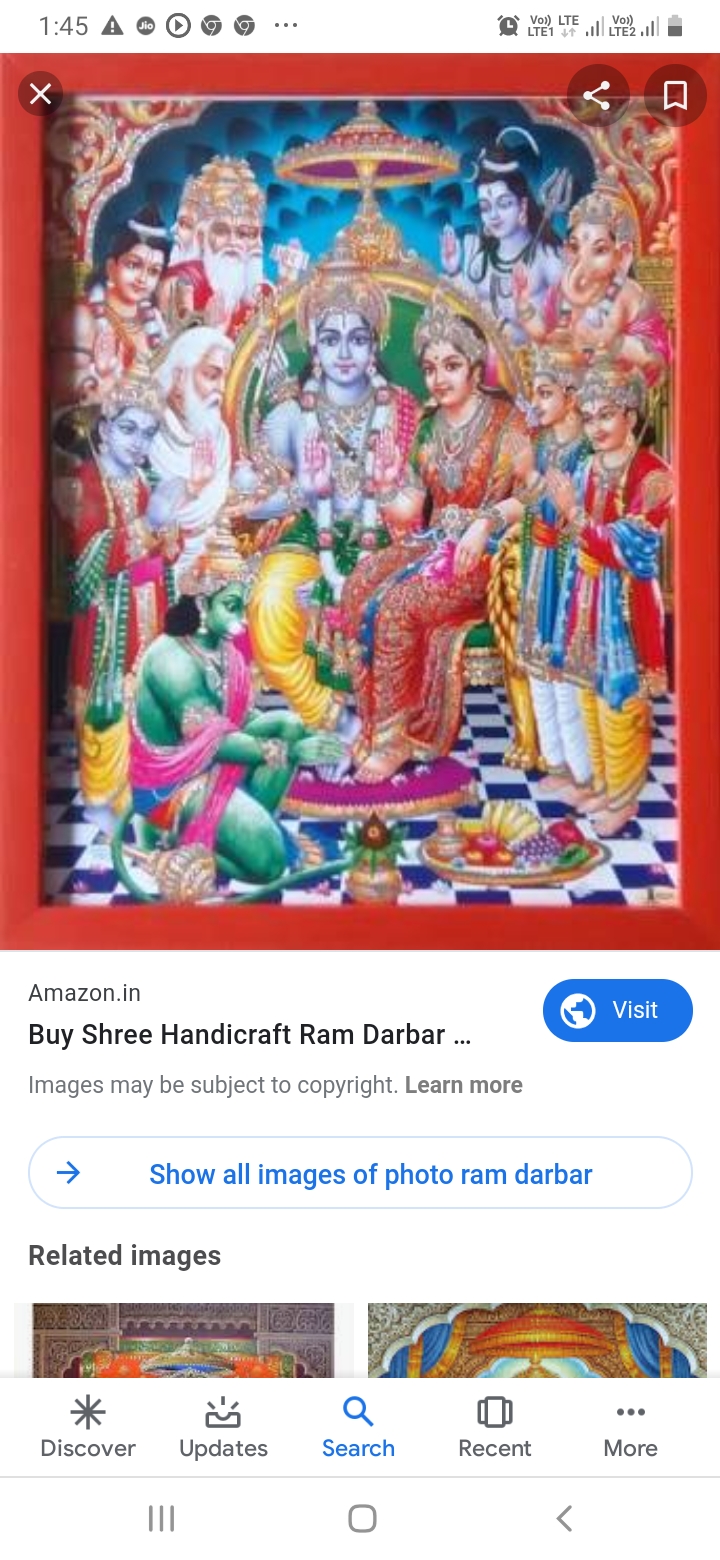भारत में जारी लॉकडाउन के बीच तीन बच्चों की माँ, उमेश चौधरी को परिवार की बुनियादी जरूरतों के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ रहा है. 37 वर्षीय उमेश दक्षिण दिल्ली के अधचिनी इलाके में रहती हैं और लॉकडाउन की वजह से उनका काम पूरी तरह से बंद हो गया है जिससे उनका घर चलता था. उमेश अपने घर के आसपास के दफ्तरों में लंच सप्लाई का काम करती हैं. वे बताती हैं, "इस काम में हमें दो पैसे बच जाते थे. दिन में करीब 35 ऑर्डर आ जाते थे और 60 रुपये एक टिफ़न की कीमत होती है. अब सारे दफ्तर बंद हैं, कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा. हम रोज़ कमाने-खाने वाले लोग हैं. पैसा जोड़ नहीं पाते. अब पाँच लोगों के परिवार को संभालना कितना मुश्किल है, कैसे बताऊं."
हालांकि भारत सरकार ने अब खेती, बैंकिग सेवाओं और सार्वजनिक कार्यों के लिए आगे बढ़ने की इजाजत दे दी है. लेकिन सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद होने से भारत के ना सिर्फ़ ग्रामीण, बल्कि शहरी हिस्सों में भी बेरोज़गारी की स्थिति और बदतर हो सकती है. आर्थिक मामलों पर गहन शोध करने के लिए जानी जाने वाली संस्था सीएमआइई का अनुमान है कि कोविड-19 की वजह से भारत में अब तक 10 से 12 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं. संस्था का कहना है कि भारत में अब बेरोज़गारी की दर 26 प्रतिशत तक पहुँच गई है.
लॉकडाउन के प्रभाव सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में बेरोज़गारी की दर में 8.7 फ़ीसद की वृद्धि देखी गई जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे ज़्यादा है. जबकि 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच यह दर बढ़कर 23.8 फीसद तक चली गई. भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रणब सेन ने कहा है कि लगभग 50 मिलियन यानी तकरीबन पाँच करोड़ भारतीय श्रमिकों की नौकरी अब तक जा चुकी है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसिज़ के चेयर प्रोफ़ेसर आर रामाकुमार ने बीबीसी से बातचीत में कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018 की तुलना में पहले ही धीमी थी. असमानता की दर भी असामान्य रूप से बढ़ी हुई थी. 2011-12 और 2017-18 के नेशनल सेंपल सर्वे के अनुसार बेरोज़गारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी हुई थी और ग्रामीण गरीबों द्वारा खाद्य सामग्री पर कम खर्च किया जा रहा था. 20172017-18 में गरीबी का स्तर पाँच फीसद तक बढ़ गया था, और ऐसी हालत में भारत को कोरोना वायरस महामारी का सामना भी करना पड़ रहा है."
प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अप्रैल के अपने संबोधन में फिर दोहराया था कि उद्योग करने वाले लोग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को नौकरियों से ना निकालें. लेकिन उद्योगपतियों और छोटे व्यापारियों की परेशानी ये है कि वे काम बंद होते हुए अपने कितने कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं. वे कहते हैं, "यूरोप और अमरीका से कोई नया ऑर्डर तो मिल नहीं रहा. और जो स्थिति है, उसे देखकर लगता नहीं कि अगले कुछ महीने तक भी हमारे पास बड़े ऑर्डर होंगे. और जितने ऑर्डर होंगे, काम के लिए लोगों की ज़रूरत भी उतनी ही होगी." विशेषज्ञों का कहना है कि उद्योगों को संभालने के लिए और अधिक राजकोषीय समर्थन की ज़रूरत है. अर्थव्यवस्था के जानकार अरुण कुमार कहते हैं कि 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज 0.8 फीसद की जीडीपी के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि क्योंकि 9 लाख करोड़ रुपये की आमदनी का नुकसान हर महीने असंगठित क्षेत्र को हो रहा है. अरुण का अनुमान है कि भारत की 94 फीसद श्रमिक आबादी देश के असंगठित क्षेत्र में काम करती है.
ग़रीबी बढ़ेगी जानकारों की मानें तो इस महामारी की वजह से देश में गरीबी बढ़ेगी क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मज़दूर यानी रोज़ कमाने-खाने की व्यवस्था और सरकारी सहायता पर आश्रित है. इस महामारी की वजह से स्थिति खराब हुई है क्योंकि देश में माँग और आपूर्ति का तालमेल बिगड़ गया है. ऐसे में भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है. छोटे और मझौले उद्योग शायद महामारी की वजह से बनी इस स्थिति स्थिति को बर्दाश्त ना कर पाएं जिसकी वजह से गरीबी बढ़ने की संभावनाएं और प्रबल होंगी.
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार ये गिरावट बहुत गंभीर होने वाली है. संगठन का अनुमान है कि भारत के असंगठित क्षेत्र में काम काम करने वाले करीब 400 करोड़ लोग पहले की तुलना में और गरीब हो जाएंगे. जानकारों की मानें तो लंबे समय तक नौकरी ना मिल पाने की समस्या को वक्त रहते नहीं सुलझाया गया तो देश में सामाजिक अशांति बढ़ेगी.
स्वतंत्र लेखक और पत्रकार रजनी बख़्शी मानती हैं कि हमें इस दर्द को दूर करने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ समान वितरण को प्रोत्साहित करना होगा. वे सुझाव देती हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस आर्थिक संकट का खामियाज़ा सिर्फ़ गरीबों को ही ना उठाना पड़े, इसलिए कुछ ठोस कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे.